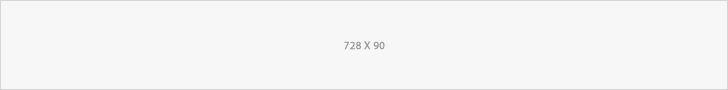ऋतुपर्ण दवे
ऋतुपर्ण दवे
नदियों को जोड़ने की मुहिम देश के लिए कितनी उपयोगी या घातक होगी, बेहद सुर्खियों में है। इसे लेकर बहुत से विशेषज्ञों की अलग-अलग राय व सरकार की अपनी योजनाएं हैं। सच्चाई यह कि प्रमाणित आधारों या अपर्याप्त उदाहरणों से संशय ज्यादा उपजा है। हर कहीं केवल अपने तर्क हैं, तर्को पर नीतियां-योजनाएं नहीं बनतीं, इसके लिए वैज्ञानिक आधार चाहिए।
तमाम विवादों और प्रकरणों के बाद सबसे पहले अब यह जरूरी हो गया है कि जितनी भी नदी जोड़ परियोजनाएं हैं, उनका वैज्ञानिक आधार सार्वजनिक हो, ताकि उपयोगी होने पर, जनसमर्थन तो मिले ही, जनजागृति भी बढ़े। लेकिन इस परिपेक्ष्य में अब तक जितनी भी बातें सामने हैं, वो बताती हैं कि योजनाओं के नफा-नुकसान पर दुविधा ज्यादा है।
जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिग के चलते भविष्य में जल की उपलब्धता और भी प्रभावित होने वाली है। नदियों में साल दर साल पानी घट रहा है। बड़ी नदियां जहां सूखती जा रही हैं वहीं गांवों, कस्बों से गुजरने वाली छोटी नदियां दम तोड़ चुकी हैं या मृत्यु शैय्या पर हैं। सबसे पहले यह सोचना होगा कि नदियों में प्रवाह कैसे बढ़े? भूजल स्तर का नाश और जल संकट से निजात की संभावनाएं तलाशनी होंगी। साथ ही सचेत भी होना पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तित हो रहे जलवायु चक्र और बढ़ रहे प्रदूषण से भी नदियां प्रभावित हैं। गंगा इसका बड़ा उदाहरण है।
हिमालयीन ग्लेशियर से आया पानी ऋषिकेश में 18 से 2 प्रतिशत के बीच रह गया है। यही कानपुर और इलाहाबाद पहुंचते-पहुंचते महज 9 से 4 प्रतिशत ही बचता है। जबकि पहले यही 54 प्रतिशत हुआ करता था। घटती बर्फबारी, पिघलते ग्लेशियर और बिगड़ते पर्यारवरणीय संतुलन से बढ़ता तापमान इसका कारण है। यद्यपि यह अलग विषय है, लेकिन जुड़े तो नदी की धारा से ही हैं।
वैसे भी नदियों को जोड़ने का काम प्रकृति का है, क्योंकि ये अपनी जलधाराएं बदलती रहती हैं। ऐसे में किसी एक जगह दो नदियों को जोड़ना कितना और कब तक उपयोगी होगा, यह भी यक्ष प्रश्न है। नदियों को जोड़ने के लिए बड़े बांधों की भी दरकार होती है।
ब्राजील के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च आईएनपीसी के एक महत्वपूर्ण शोध से इस बात का भी खुलासा हुआ है कि दुनिया भर के बड़े बांध, हर वर्ष 104 मिलियन मीट्रिक टन मीथेन गैस उत्सर्जित करते हैं जो ग्लोबल वार्मिग में मानव जनित हिस्से का चार प्रतिशत है।
दुनिया भर में यह चर्चा का विषय है। इन सबके बीच नदी और जल को बचाने, सार्थक और प्राकृतिक तरीकाए जल प्रबंधन ही प्रभावी व सफल दिखता है। इसके लिए बहुत छोटे से देश इजरायल से सीखना होगा। भारत के क्षेत्रफल की तुलना में केवल 0.63 प्रतिशत भूभाग अर्थात 20770 वर्ग किलोमीटर वाले इस देश में केवल दो प्रतिशत भूभाग में पानी है जबकि भारत में 9.5 प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्रफल पानीदार है।
बारिश भी वहां भारत से औसतन 215 मिमी कम होती है। लेकिन वहां पानी की बचत और रिसाइक्लिंग के लिए कई प्रभावी उपाए हुए। कारखानों में सीमित मात्रा में ऐसे तत्वों, अवयवों के उपयोग पर सख्ती हुई जो प्रदूषण के जनक हैं। इसके अलावा रिसाइकल्ड पानी खेतों में उपयोग किया जाने लगा। नतीजन वहां मांग का 93 प्रतिशत अन्न खुद ही पैदा किया जाने लगा।
नदियों में आने वाली गाद की मात्रा, नहर परियोजनाओं के अनुभव और विदेशों में ऐसी परियोजनाओं की गति पर भी गौर करना जरूरी होगा। तभी भविष्य की तमाम शंकाओं-कुशंकाओं का निवारण हो सकेगा।
भारत में हाल में बिहार में बाढ़ की तबाही इसका सबसे ज्वलंत उदाहण है, जिसके लिए, वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पश्चिम बंगाल में गंगा पर बने फरक्का बैराज और शहडोल में बने बाणसागर बांध को जिम्मेदार मानते हैं।
फरक्का से गंगा की जल निकासी में कमी से गाद जमा होने लगी, जिससे नदी तल प्रभावित हुआ। इधर बाणसागर बांध के संचालन में लापरवाही से पानी एकाएक बढ़ा और बिहार में 14 प्रतिशत कम बारिश के बावजूद बाढ़ का अभूतपूर्व मंजर दिखा।
बहरहाल, मांग तो यह भी हो रही है कि देश भर में 12 नदियों गंगा, यमुना, कावेरी नर्मदा, दामोदर, ताप्ती, मघा, सिंधु, सतलज, गोदावरी, ब्रम्हपुत्र और कृष्णा जिनका दायरा लगभग 15895 किलोमीटर है, को आपस में जोड़ने की परियोजना शुरू हो।
इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में इसी नौ जून को चेन्नई के 65 वर्षीय गजेंद्रन ने एक जनहित याचिका दायर कर दिल्ली से कोलकता, ओडिशा, विजयवाड़ा होकर चेन्नई तक की चार हजार किमी लंबी साइकल यात्रा शुरू की है। निश्चित रूप से विविध विचारों, धारणाओं और मांग के बीच जरूरी यह है कि नदियों की स्वतंत्रता छीनने, उसकी अविरल धारा से छेड़खानी करने के पहले उसके नतीजों पर व्यापक सोच, शोध और वैज्ञानिक आधारों हों। महज वातानुकूलित कमरों में बैठकर कागजों में ड्राइंग बना देने से योजनाएं सफल नहीं होती हैं।
यह भी एक अजब संयोग है कि एक ओर पेरिस जलवायु परिवर्तन पर अमल करने और कार्बन उत्सर्जन कम करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर केन-बेतवा को जोड़ने का फैसला होता है।
कुछ भी हो दुनिया भर के तमाम देशों के प्रयोगों, शोध, नीति निर्देशकों, उदाहरणों का पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से अध्ययन के बाद ही भारत जैसे विशाल भू-भाग और जनसंख्या वाले देश में ऐसी परियोजनाएं लागू की जाएं, क्योंकि इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि अगला विश्व युद्ध पानी को लेकर होना तय है। जनसंख्या की ²ष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश भारत, जहां दुनिया की 18 प्रतिशत आबादी रहती है, लेकिन पानी का भंडार केवल चार प्रतिशत।
उससे भी बड़ा सच यह है कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, नदियों के किनारे अतिक्रमण, प्राकृतिक संपदाओं के अकूत दोहन से करोड़ों क्यूसेब पानी समुद्र में चला जाता है। इसलिए अव्वल जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले हम जल प्रबंधन पर ध्यान दें। नदियों को जोड़ने से ज्यादा जरूरी है कि लोगों को सामाजिक और भावनात्मक तौर पर नदियों से जोड़ा जाए। नदी के महत्व और भविष्य की आवश्यक्ताओं को बताया जाए।
जरूरी है कि लोगों को आसन्न जलसंकट और बिन पानी सब सून की भयावहता से रू-ब-रू कराया जाए, ताकि प्राकृतिक जलस्रोतों का जाने-अनजाने विभिन्न कारणों से दुश्मन बना इंसान चेत जाए। यदि समय रहते इस सच्चाई को जन-जन तक नहीं पहुंचाया गया तो योजनाएं चाहें कोई भी हों, व्यर्थ हैं, धन अपव्यय और भृष्टाचार का निवाला से ज्यादा कुछ नहीं है।
अहम जरूरत यह है कि दम तोड़ती नदियों को बचाएं, मर चुकी नदियों को पुनर्जीवित करें। ताल-तालाबों, पोखरों को सहेजें उन्हें फिर उन्नत और लबालब करें। उससे भी जरूरी यह कि गंदे जल की निकासी के लिए वैज्ञानिक ²ष्टिकोण अपनाएं तभी संभव है कि हम नदियों को उनका अपना मूल स्वरूप लौटा पाएंगे और जब यह सब कर लेंगे तो शायद, करोड़ों-अरबों खर्च कर नदियों को जोड़ने की जरूरत ही न रह जाए।
इसके लिए जन जागृति, संचार-संवाद के मौजूदा हाईटेक जमाने में बड़ी ही सहजता से लोगों को जोड़ा जा सकता है। इसे मीडिया, सोशल मीडिया, संवाद-विचार गोष्ठियों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एक ईमानदार संकल्प के रूप में किया जा सकता है। काश! इस सबकी तरफ भी हमारे नुमाइंदे नजरें इनायत कर पाते। (आईएएनएस)
(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके निजी विचार हैं)