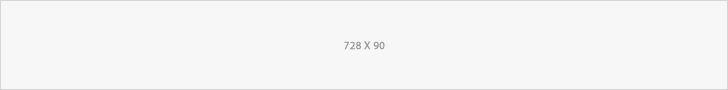लखनऊ, 22 फरवरी (आईएएनएस/आईपीएन)। प्रकृति सुकृति है। तार्किक वैज्ञानिक संरचना-इंटेलीजेंट डिजाइन। इसका दृश्यमान भाग ‘सत्’ कहा गया है। प्रत्यक्ष सत्य। इसका अदृश्य मगर अनुभूति सिद्ध भाग असत्। असत् असत्य नहीं है। सत् और असत् वैदिक साहित्य में हैं। सत् व्यक्त है और असत् अव्यक्त।
लखनऊ, 22 फरवरी (आईएएनएस/आईपीएन)। प्रकृति सुकृति है। तार्किक वैज्ञानिक संरचना-इंटेलीजेंट डिजाइन। इसका दृश्यमान भाग ‘सत्’ कहा गया है। प्रत्यक्ष सत्य। इसका अदृश्य मगर अनुभूति सिद्ध भाग असत्। असत् असत्य नहीं है। सत् और असत् वैदिक साहित्य में हैं। सत् व्यक्त है और असत् अव्यक्त।
प्राकृतिक नियम दिखाई नहीं पड़ते। प्रकृति के अंश, रूप और गति देखकर हम नियमबद्धता का अनुभव करते हैं। समय भी नहीं दिखाई पड़त। सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच एक अहोरात्र (दिनरात) का अनुभव कालगणना देता है। वैदिक पूर्वजों ने प्रकृति के अंतस्थल मंे विद्यमान संविधान को ठीक से जान लिया था। ऋतुएं इस संविधान का प्रत्यक्ष रूप हैं।
उन्होंने इस संविधान का नाम ऋत रखा था। पूर्वजों ने नदियों को ऋतावरी गाया। नदियां ऋत संविधान का पालन करती हैं। अग्नि, भी ऋत अनुसरण वाले कहे गए। इंद्र की क्षमता का रहस्य ऋत संविधान का पालन करना था। ऋत से बड़ा कोई नहीं। ईश्वर भी इस संविधान से ऊपर नहीं।
प्राकृतिक नियमों में हस्तक्षेप उसकी भी क्षमता से परे बताया गया। वैदिक समाज ने इसी नियम पालन का नाम धर्म रखा। जो प्रकृति के भीतर ऋत है वही मनुष्य के लिए धर्म है। प्रकृति संविधान का पालन कर्तव्य है और यही कर्तव्य धर्म जाना गया।
धर्म प्राकृतिक नियमों के अनुसरण की आचार संहिता है। वैज्ञानिकों ने ब्रह्माण्ड रहस्यों के शोध पर बड़ा काम किया है। अब तक प्राप्त निष्कर्षो में समूची सृष्टि परस्पर अंर्तसबंधित एक एकात्म ही जानी गई है।
वैज्ञानिक शोध और ऋषि बोध लगभग एक जैसे हैं। ऋषि बोध में ‘एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति’ की घोषणा है तो विज्ञान शोध में समूचे विश्व – कासमोस को एक जानने के निष्कर्ष। शोध और बोध एक जैसे हैं।
समग्र-संपूर्ण को अपने अंतस्थ में अनुभव करना बोध है और अलग-अलग इकाइयों परमाणुओं, ऊर्जा तरंगों को परस्पर एक देखना समझना शोध। भारत के धर्म ने शोध को बोध का विराट लक्ष्य दिए हैं। शोध ज्ञान देता है, आत्मीयता नहीं देता। बोध ज्ञान के साथ आत्मीयता भी देता है। बोध स्वयं को विराट का अंश जानने की अनुभूति है।
बोध आत्यंतिक विनम्रता है और शोध आत्यंतिक आक्रामकता। पूर्वजों ने शोध को बोध का उपकरण बनाया था। धर्म के ऐसे ही अनेक उदात्त लक्ष्य रहे हैं। ऐसा सब प्रत्यक्ष और स्वयं सिद्ध होने के बावजूद यूरोपीय विद्वानों ने भारत को जादू टोने आदि अविश्वसनीय कर्मकांडों का अंधविश्वासी समाज बताया। भारतीय धर्म को अंधविश्वासी बताने के पीछे ईसाई पंथ प्रचार के उद्देश्य भी थे।
ऋग्वेद प्राचीनतम शब्द साक्ष्य है। भारतीय दर्शन समाज संगठन और मानवीय आचार व्यवहार का प्रीतिपूर्ण दिग्दर्शन। जान पड़ता है कि वैदिक काल में भी जादू टोने का प्रचलन था। ठगी भी रही होगी। लेकिन ऋग्वेद के ऋषि ऐसे कृत्यों के निन्दक थे। ऐसे कर्मकांडियों को ‘अनृतदेवों’ का उपासक कहा गया है। ‘अनृतदेव’ ध्यान देने योग्य है। जो ऋत नहीं है वही अनृत है।
प्रकृति के संविधान ऋत के विरोधी हैं अनृतदेव। यहां शिश्नदेव उपासकों को मार भगाने की भी स्तुति है। ऋग्वैदिक पूर्वज ‘यातुधान’ करने वाले और राक्षस कर्म वाले उपासकों के विरोधी थे।
वैदिक भाषा का ‘यातु’ शब्द हमारी भाषा का जादू है। ऋग्वेद के 7.104 व 10.87 सूक्त पठनीय हैं। संभवत: स्त्रियां भी जादू आदि कर्मकांड करती थीं। ऋग्वेद में इंद्र से ‘रक्तिम पिशाचिनी को’ दंडित करने की स्तुति है। वैदिक समाज अंधविश्वासी नहीं था।
संप्रति तमाम संचार माध्यमों/टीवी चैनलों में अंधविश्वासी कर्मकांडों का धुआंधार प्रचार है। बिगड़े प्रेम संबंधों को ठीक कराने व धन संपदा दिलाने की अंधविश्वासी घोषणाएं हैं। ठगी चालू है लेकिन भारतीय धर्म साधना से इनका कोई संबंध नहीं है।
वैदिक समाज अंधविश्वासी नहीं था। यातुधान- जादुई कर्म या अभिचार कर्म अंधविश्वासी थे। तुलसीदास ने भी यातुधान शब्द का प्रयोग किया है। वैदिक समाज में यातुधान की निंदा थी। वशिष्ठ ऋग्वेद के प्रमुख मंत्रद्रष्टा हैं। ‘˜यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम’ उनका ही रचा गया लोकप्रिय मंत्र छंद है। बहुत बाद में इसे महामृत्युंजय मंत्र की संज्ञा मिली।
जान पड़ता है कि किसी ने वशिष्ठ को ‘अभिचार कर्मी’ कह दिया था। ऋग्वेद (7.104.15-16) में वशिष्ठ की व्यथा है “मैं आज ही मृत्यु को प्राप्त होंऊ यदि मैं अभिचार (जादू – टोना) प्रयोग करने वाला होऊं। मुझ पर झूठा आरोप लगाने वाला अपने पुत्रों से रहित हो जाए।” तब अभिचार कर्म भी गाली जैसा था। अभिचार कर्म का आरोप अस था।
यूरोपीय विद्वानों और कुछेक भारतीय लेखकों ने भी भारतीय धर्म परंपरा पर अंधविश्वासी होने के ऐसे ही आरोप लगाए हैं लेकिन हम विश्वामित्र और वशिष्ठ की परंपरा में आहत नहीं होते। वशिष्ठ मरूद्गणों से गुहार करते हैं “हे मरूतो! तुम सब तरफ व्याप्त हो जाओ। विभिन्न रूप धरे इन दुष्टों को पकड़ लो और दण्डित करो।” अंधविश्वासी अभिचारकर्मी यातुधानी तब निंदनीय ही नहीं दंडनीय भी थे। वैदिक धर्म मंे अंधविश्वास की कोई मान्यता नहीं थी।
भारतीय धर्म परंपरा अंधविश्वास नहीं है। इस परंपरा के विकास की लंबी यात्रा है। वैदिक साहित्य में पूर्ववर्ती समाज के भी संकेत हैं। ऋषि अपने काव्य को नए स्तोत्र की संज्ञा देते हैं। स्तुति परंपरा का भी उल्लेख करते हैं। इस परंपरा में तर्क आधारित दर्शन है तो अनुभूति आधारित भाववाद भी है।
सबसे बड़ी बात है प्रकृति के रूपों के प्रति सजगता और उनके गुण धर्म को तात्विक ²ष्टि से समझने की व्यग्रता। वे सूर्य, चंद्र, अग्नि और अंतरिक्ष सहित पशु पक्षी कीट पतिंग तक को अपने अध्ययन और काव्य सृजन का विषय बनाते हैं। अध्ययन और निष्कर्ष की इस शैली में अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। वे आधुनिक वैज्ञानिक भौतिकवादी से भी ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले हैं और कांट से भी ज्यादा तार्किक मीमांसक भी।
वे ढोंगी आधुनिक सेकुलर वादियों से बड़े वास्तविक इहलोकवादी हैं। ऋग्वेद में वशिष्ठ के सूक्त प्राय: 7वें मंडल में हैं। दसवां मंडल बाद का माना जाता है। यहां अंधविश्वासी कर्मकांड से जुड़े यातुधान को जड़मूल से समाप्त करने की प्रार्थना है “हे अग्नि! यातुधान के टुकड़े-टुकड़े करो। तुम्हारा ताप उसे जलाए, मार डाले। जो मूर्ख – देवों के उपासक हैं, वे सूर्योदय न देखें।”
यहां अंधविश्वासी कर्मकांडों के देवों को भी मूर्ख बताया गया है। वैदिक समाज की इसी परंपरा में भारतीय दर्शन धर्म और संस्कृति का विकास हुआ है।
कुछेक विद्वानों ने अंधविश्वासी कर्मकांडों को तंत्र के विकास से जोड़ा है। निस्संदेह यहां तंत्र का विकास भी हुआ, लेकिन ऋग्वैदिक काल में तंत्र परिपाटी के साक्ष्य नहीं मिलते। तंत्र शब्द को ‘तन्व त्रै’ धातु से बना बताया जाता है। यहां तन्व का अर्थ है फैलाना, तानना और त्रै का अर्थ है संरक्षण। गीता का ‘परित्राणाय’ संरक्षण देने का ही बोध देता है।
त्राण संरक्षण है और परित्राण संपूर्ण संरक्षण। ऋग्वेद में तंत्र का अर्थ कपड़ा बुनने और कृषि उपकरणों के लिए आया है। शंकराचार्य ने इस शब्द का उपयोग सिद्धांत के लिए किया। उन्होंने वेदांत सूत्रों के भाष्य में सांख्य दर्शन को सांख्य तंत्र व पूर्व मीमांसा को प्रथम तंत्र कहा है। तंत्र का अर्थ अंधविश्वास नहीं था।
लोकतंत्र या जनतंत्र में भी तंत्र सिद्धांत या संगठित उपकरण की ही ध्वनि देता है। तंत्र की तरह मंत्र भी मन्व और त्रै का निर्माण होना चाहिए। मंत्र का अर्थ है चंचल और विस्तारित मन का संरक्षण। वैदिक परम्परा मंत्र प्रधान है। मंत्र का अर्थ परामर्श भी होता है। मंत्र की शक्ति अपरंपार है। जनतंत्र के मंत्री की शक्ति ध्यान देने योग्य है।
मूलतत्व है – द्रष्टा भाव। यही ऋषि तत्व है और इसमें अंधविश्वासी नहीं है। भारतीय धर्म को अंधविश्वास बताने वाले निरे अंधविश्वास ही हैं।
(लेखक हृदयनारायण दीक्षित चर्चित स्तंभकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं)