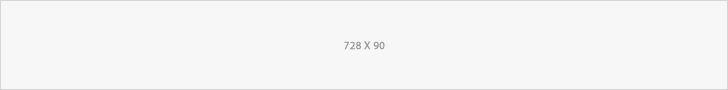अंग दान और अंग प्रत्यारोपण हर साल हजारों लोगों को नई जिंदगी देता है। अमीरों और गरीबों की बीच बढ़ती खाई, मानव अंगों की मांग और तकनीक की उपलब्धता ने अंगों के व्यापार को कुछ लोगों के लिए धन कमाने का साधन बना दिया है तो कुछ के लिए राहत की राह भी तैयार कर दी है। लेकिन अमूमन अंगों का व्यापार गरीबी में फंसे लोगों के शोषण का जरिया बन जाता है। पैसों की तत्काल जरूरत पूरी करने के लिए वे अंग बेचने को मजबूर हो जाते हैं।
अंग दान और अंग प्रत्यारोपण हर साल हजारों लोगों को नई जिंदगी देता है। अमीरों और गरीबों की बीच बढ़ती खाई, मानव अंगों की मांग और तकनीक की उपलब्धता ने अंगों के व्यापार को कुछ लोगों के लिए धन कमाने का साधन बना दिया है तो कुछ के लिए राहत की राह भी तैयार कर दी है। लेकिन अमूमन अंगों का व्यापार गरीबी में फंसे लोगों के शोषण का जरिया बन जाता है। पैसों की तत्काल जरूरत पूरी करने के लिए वे अंग बेचने को मजबूर हो जाते हैं।
हर साल सैकड़ों भारतीय अंग प्रत्यारोपण के इंतजार में मर जाते हैं। इसकी वजह है अंग दान करने वालों और प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहे लोगों के बीच जबर्दस्त असंतुलन। हर साल 2.1 लाख भारतीयों को गुर्दा प्रत्यारोपण की जरूरत होती है लेकिन सिर्फ 3000 से 4000 गुर्दा प्रत्यारोपण ही हो पाते हैं। हृदय प्रत्यारोपण के मामले में भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। देश में हर साल 4000 से 5000 लोगों को हृदय प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ती है लेकिन अब तक सिर्फ 100 लोगों का ही हृदय प्रत्यारोपण हो सका है।
नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस- एनपीसीबी की 2012-13 की रिपोर्ट के मुताबिक 2012-13 के दौरान देश में 4,417 कॉर्निया उपलब्ध थे, जबकि हर साल 80,000 से 1,00,000 कॉर्निया की जरूरत होती है। देश में इस समय 120 प्रत्यारोपण केंद्र हैं, जहां हर साल 3500 से 4000 गुर्दा प्रत्यारोपण किए जाते हैं। इनमें से चार केंद्रों पर 150 से 200 यकृत (लीवर) प्रत्यारोपण होते हैं। जबकि कुछ केंद्रों पर कभी-कभी एकाध हृदय प्रत्यारोपण हो जाता है।
अंग प्रत्यारोपण की दिशा में सबसे बड़ी दिक्कत अंग दान दाताओं का अभाव है। जागरूकता की कमी और अंग दान और प्रत्यारोपण के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना न होने की वजह से अंग प्रत्यारोपण की गति धीमी है। लोगों के बीच इसे लेकर कई सारे मिथक भी हैं और अंग प्रत्यारोपण की दिशा में आने वाली अड़चनों को खत्म करने के लिए इन्हें समाप्त किया जाना भी जरूरी है। बड़ी संख्या में भारतीयों का कहना है अंगों की कांट-छांट या उन्हें शरीर से अलग करना प्रकृति और धर्म के खिलाफ है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर उन्हें अंग प्रत्यारोपण कराना हो तो अस्पताल के कर्मचारी उनकी जिंदगी बचाने के लिए मेहनत नहीं करेंगे।
कुछ का मानना है कि मरने से पहले ही उन्हें मृत घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा अंग दान की गतिविधियों का केंद्रीकृत रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था का न होने से भी लोगों को अंग दान करने वालों के बारे में आंकड़े नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा ब्रेन डेथ को प्रमाणित करने की समस्या भी पैदा होती है। अगर लोगों को ब्रेन डेथ के बारे में पता नहीं है तो मरीज के परिजनों को अंग दान करने के लिए समझाना मुश्किल होता है।
भारत में 1970 में गुर्दा प्रत्यारोपण शुरू हो गया था और इसके बाद यह एशियाई महाद्वीप में इस मामले में अग्रणी बना हुआ है। पिछले चार दशक के प्रत्यारोपण विकास के इतिहास के दौरान देश में अंग दान का कारोबार भी अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बन गया है। सरकार ने 1994 में मानव अंग प्रत्यारोपण (टीएचओ) अध्यादेश पारित किया था। इस कानून के तहत असंबद्ध प्रत्यारोपण को गैरकानूनी बना दिया और मस्तिष्क की मृत्यु (ब्रेन डेथ) की स्वीकृति मिलने के बाद मृतक के अंग दान को कानूनी करार दिया।
जिन मरीजों के मस्तिष्क की मृत्यु हो चुकी थी उनकी संख्या को इकट्ठा कर अंगों की कमी की चुनौती से पार पाने और असंबद्ध प्रत्यारोपण गतिविधियों को रोकने की उम्मीद लगाई गई थी। लेकिन टीएचओ कानून से न तो अंगों का व्यापार रूका और न ही वैसे मरीजों की संख्या बढ़ी जिन्होंने मस्तिष्क की मृत्यु की स्थिति में अंग दान कर दिया हो। दरअसल मरीज की मस्तिष्क की मृत्यु (ब्रेन डेथ) की अवधारणा को न तो कभी बढ़ावा मिला और न ही इसे व्यापक तौर पर प्रचारित किया गया। इस समय प्राधिकार कमेटी की मंजूरी के बाद ज्यादातर असंबद्ध प्रत्यारोपण किए जा रहे हैं।
सरकार ने 2011 में मानव अंग प्रत्यारोपण से संबंधित संशोधन कानून लागू किया, जिसमें अंग दान की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रावधान मौजूद थे। कानून के प्रावधानों में अंग दान करने वाले मृतक से अंग हासिल करने के केंद्र और निबंधन कार्यालय बनाने की व्यवस्था शामिल हैं। साथ ही अंगों की अदला-बदली रजिस्टर्ड चिकित्सक की ओर से प्रत्यारोपण समन्वयक (को-ऑर्डिनेटर, अगर कोई हो तो) से सलाह-मशविरा कर अनिवार्य करने का नियम शामिल है।
निकट के रिश्तेदारों से भी सलाह-मशविरा और सघन चिकित्सा केंद्र में भर्ती संभावित दानदाता और अगर वे राजी हों तो उन्हें अंग दान के विकल्प के बारे में जानकारी देना जैसा नियम भी शामिल है। इसके अलावा दानदाताओं को अंग निकाले जाने वाले केंद्रों के बारे में जानकारी देना का नियम भी शामिल है।
भारत में मृतक की ओर से अंग दान की भारी संभावना है, क्योंकि यहां भारी संख्या में जानलेवा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। किसी भी समय हर प्रमुख शहर के सघन चिकत्सा केंद्रों में आठ से दस ब्रेन डेथ के मामले होते ही हैं। अस्पतालों में होने वाली मौतों के मामले में चार से छह फीसदी ब्रेन डेथ के ही होते हैं। भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 14 लाख लोगों की मौत हो जाती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली के अध्ययन के मुताबिक इनमें से 65 प्रतिशत लोगों के मस्तिष्क में चोट लगी होती है। इसका मतलब यह है कि 90,000 लोग मामले ब्रेन डेथ के हो सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि भारत में लोग अंग दान नहीं करना चाहते लेकिन अस्पतालों में ब्रेन डेथ की पहचान करना और उनके प्रमाणन का कोई तंत्र मौजूद नहीं है। इसके अलावा कोई भी मृतक के रिश्तेदारों को मरीज के अंग को दान देकर अन्य लोगों की जीवन रक्षा का अधिकार नहीं देता। कोई भी व्यक्ति, बच्चे से से लेकर बड़े तक अंग दान कर सकता है। जिस व्यक्ति की मस्तिष्क की मृत्यु हो चुकी हो और जिसे मृत्यु बाद अंग दान कहा जाता है वह अभी भारत में बहुत कम है। स्पेन में प्रति दस लाख लोगों पर अंग दान करने वाले 35 लोग हैं। ब्रिटेन में यह संख्या प्रति दस लाख लोगों पर 27, अमेरिका में 11 है। लेकिन भारत में प्रति दस लाख लोगों में अंगर दान करने वाले सिर्फ 0.16 व्यक्ति हैं।
अगर अंग दान करने की इच्छा तो इस दिशा में दानदाता कार्ड पर हस्ताक्षर करना पहला कदम है। दानदाता कार्ड कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है लेकिन यह किसी व्यक्ति के अंग दान की इच्छा को दशार्ता है। जब कोई व्यक्ति अंग दान दाता कार्ड पर हस्ताक्षर करता है तो यह उसके अंग दान की इच्छा को जाहिर करता है और इस बारे में उसके निर्णय को उसके परिवार के लोगों या दोस्तों को बताना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंग दान के लिए परिवार के सदस्यों को सहमति देने के लिए कहा जाएगा।
मस्तिष्क की मृत्यु होने की स्थिति में महत्वपूर्ण अंग जैसे यकृत, फेफड़ा, गुर्दा, अग्नाशय, आंत, उत्तक जैसे कॉर्निया, हृदय के वाल्व, त्वचा, हड्डी, अस्थि संधि, शिरा और नस को दान किया जा सकता है। (आईएएनएस/आईपीएन)