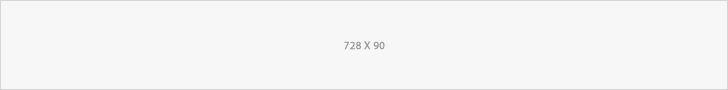जनतंत्र सामूहिक प्रीति रीति है। मनुष्य की सामासिक योजकता। हरेक मनुष्य अद्वितीय है। अनूठा। उस जैसा दूसरा नहीं। अप्रतिम और अतुलनीय। भिन्न विचार, भिन्न विश्वास और भिन्न भिन्न भाषा बोली। सबके रूप, रंग, छन्द भिन्न भिन्न हैं। निवास की दृष्टि से भूक्षेत्र और परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न हैं। लेकिन परस्पर प्रीति सनातन भारतीय प्यास है।
जनतंत्र सामूहिक प्रीति रीति है। मनुष्य की सामासिक योजकता। हरेक मनुष्य अद्वितीय है। अनूठा। उस जैसा दूसरा नहीं। अप्रतिम और अतुलनीय। भिन्न विचार, भिन्न विश्वास और भिन्न भिन्न भाषा बोली। सबके रूप, रंग, छन्द भिन्न भिन्न हैं। निवास की दृष्टि से भूक्षेत्र और परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न हैं। लेकिन परस्पर प्रीति सनातन भारतीय प्यास है।
भारतीय स्वप्न है कि सब अपने रस, छंद और लय में जिएं, लेकिन सबके मन समान हों। सबका प्रकाश एक साथ चमके। सभा ऐसी ही संस्था है। सभा में ‘स’ सहित का सूचक है और ‘भा’ प्रकाशवाची है ही। म्यांमार, नैपाल और चीन जैसे पड़ोसी भूखण्ड जनतंत्री नहीं हो सके। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र हो गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारतीय संस्कृति से जुड़े होकर भी प्राचीन जनतंत्री भावभूमि नहीं अपना सके।
समाजशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों और राजनेताओं के लिए यह विषय महत्वपूर्ण चुनौती है। प्रश्न बड़ा है। आखिरकार तमाम विविधताओं के बावजूद भारत क्यों जनतंत्री है? और पड़ोसी देशों में प्रीतिपूर्ण जनतंत्र का विकास क्यों नहीं हो पाया? भारतीय चिन्तन की मूल भूमि लोकतंत्र है। लोक और जन वैदिक पूर्वजों के प्रियतम विचार रहे हैं।
लोक बड़ा है। आयतन में असीम लेकिन विश्वास में हृदयग्राही। लोक प्रकाशवाची है। भारतीय चिंतन में लोक एक नहीं अनेक हैं। यजुर्वेद के अंतिम अध्याय में कई लोकों का उल्लेख है, ‘असूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता: – असुरों के अनेक लोक हैं। वे अंधकार से आच्छादित हैं। आत्मविरोधी इन्हीं में बारंबार जाते हैं।’ यहां अज्ञान अंधकार आच्छादित लोक का वर्णन है। इसके पहले ऋग्वेद के पुरूष सूक्त में भी कई लोकों का उल्लेख है। यहां ‘पुरुष’ संपूर्णता का पर्याय है।
कहते हैं, “यह विश्व उस पुरुष की महिमा है। झलक मात्र है। पुरुष इससे बड़ा है। विश्व उसका एक भाग (पाद) है। तीन भाग अमृत लोक में हैं।”
जान पड़ता है कि अमृतलोक का आयतन इस विश्व से तीन गुना बड़ा है। जो भी हो ‘लोकों’ की धारणा वैदिक काल से ही गतिशील नदी की तरह समूचे जनजीवन में जस की तस बह रही है। मृत्यु की सूचना के बाद शोकग्रस्त लोग मृत्युलोक, पितरलोक, स्वर्गलोक आदि की चर्चा करते हैं।
यहां सामान्य चर्चा में भी ‘लोक’ आ जाता है। यह ‘लोक’ शास्त्र का भी अतिक्रमण करता है। कर्मकांड की तमाम विधियों में शास्त्रीय रीति को काटने वाले लोग नई रीति को लोकरीति कहते हैं। इस अर्थ में लोक का अर्थ सामान्यजन होता है। शास्त्रीय गीत और संगीत की जगह लोकगीत या लोकसंगीत ऐसी ही प्रिय धारणाएं हैं।
लोक का अर्थ केवल मनुष्य नहीं। जन का अर्थ केवल एक मनुष्य नहीं। जन-समूह ही है। ऋग्वेद सहित समूचे वैदिक साहित्य में लोक का अर्थ जन से बड़ा है। जन की महत्ता भी कम नहीं। ऋग्वेद के अदिति देव का विस्तार बताते हुए ऋषि ने ‘अदिति पंचजना : – अदिति 5 जन’ का शब्द प्रयोग किया है। ऐतरेय उपनिषद् ऋग्वेद संबंधी है। यहां ‘आत्मा’ को सृष्टि सृजन का कर्ता बताया गया है।
इस उपनिषद् के प्रारंभ में कहते हैं कि आदि में आत्मा अकेला था, दूसरा कोई नहीं था – आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत। नान्यत्किंचनमिषत। उसने लोकसृजन की इच्छा की – स ईक्षत लोकन्नु सृजा इति। उसने लोक बनाए – स इमांलोकन्नु सृजत। उसने द्युलोक और ऊपर के लोक, जल के नीचे के लोक, स्वर्ग लोक और उसके ऊपर के लोक बनाए। यहां भी अनेक लोकों का उल्लेख है।
उसने लोकपाल भी बनाए और सबके लिए अन्न भी – अन्नामेभ्य: सृजा इति। यहां आत्मा के द्वारा लोक बनाने को अलग कर दे तो सृष्टि का विकासवादी सिद्धांत स्पष्ट हो जाता है। लोक अनेक हैं। तुलसी की कथा के गरुड़ – कागभुशुण्डि संवाद में भी अनेक लोक हैं। वैज्ञानिक अनेक सौर परिवारों की बाते कर रहे हैं। ऋग्वेद में सूर्य लोक और चंद्र लोक हैं ही। जन से लोक बड़े हैं। तब जनतंत्र से लोकतंत्र भी बड़ा और व्यापक होना चाहिए।
विश्व एक व्यवस्था है। सुंदर, अच्छी, बुरी, अनुशासित या अराजक? जैसी भी। कैसी भी। व्यवस्था तो है ही। आदि मानव ने परिस्थितिवश अपने समुदाय बनाए। समुदायों ने आंतरिक अनुशासन गढ़े। आत्म-अनुशासन के बावजूद उजड्ड लोग अपनी राह चले। इसी परिस्थिति में राजा या राजव्यवस्था का जन्म हुआ। भारत में समूह या समुदाय की सबसे सुंदर इकाई थी परिवार। बहुत छोटी लेकिन सर्वांग सुंदरी। परिवार स्वाभाविक इकाई है। इसके बाद की इकाइयां परिस्थितिवश अस्तित्व में आईं। बाद में इकाइयों में परिवार भाव के विकास की प्यास निरंतर बनी रही।
‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भारतीय आकांक्षा में भी यही प्यास है। भारत में परिवार के बाद सबसे छोटी इकाई बनी गण। गण वस्तुत: अंत: संगठित समूह थे। गण के नेता गणपति, गण अध्यक्ष आदि कहे गए और आस्था में गणेश भी। गणेश संभवत: इसीलिए सभी पूजनीयों में प्रथम हैं और सभी देवों में अग्रगण्य भी। गण समूह सांस्कृतिक आर्थिक और अन्य कारणों से आपस में मिलते गये। गणों से मिलकर बड़ी इकाई बनी ‘जन’। भारतीय राष्ट्रगान में जन के साथ गण भी हैं और जनगण का सामूहिक मन ही जनगणमन है। जनगणमन की सामूहिकता ही जनतंत्र है।
जनतंत्र मानव समाज की आंतरिक एकता है। यह आंतरिक एकता अर्जित करनी होती है। लोकतंत्र स्वाभाविकता है। हम प्रकृति के अंग हैं, पृथ्वी के अंग हैं, जल, अग्नि, वायु और आकाश के अंग हैं। परिवार के अंग हैं और समाज के भी अंग हैं। किसी राजनैतिक दल के सदस्य होने के कारण दल के भी अंग हैं। समिति या अन्य संस्थाओं के भी अंग होते हैं। मनुष्य सोचता है।
हम सब चिंतनशील प्राणी हैं। पशु और वनस्पतियां भी प्राण ऊर्जा से भरी पूरी हैं। वे भी चिंतनशील हैं। जनतंत्र की सफलता के लिए सबके प्रति अपने दायित्व का चिंतन जरूरी है। पश्चिम के जनतंत्र और भारतीय जनतंत्र में यही मौलिक अंतर है। वे केवल मनुष्य के बारे में सोचते हैं।
भारत मंे सृष्टि के सभी अवयवों पर समग्र विचार की परंपरा है। यहां जन के साथ लोक का भी विचार चलता है। पश्चिम का जनतंत्र राजतंत्र की प्रतिक्रिया है। भारतीय जनतंत्र हमारे रस, रक्त प्रवाह का हिस्सा है। यहां का जन लोक से रस लेता है। लोक को सींचता है, स्वयं भी रससिक्त है। लोक प्रीतिकर है, जन प्रीति इसी अनुभूति का अनुषंग है। जनतंत्र लोकतंत्र का पुत्र है।
लोकतंत्र में सूर्य चंद्र नदी, पर्वत, कीट, पतिंग, वनस्पति, पशु और मनुष्य भी सम्मिलित हैं। क्या हम तमाम लोकों का अस्तित्व स्वीकार कर सकते हैं? चिंतन की अल्प अवधि के लिए ऐसा सोचना बुरा नहीं। तब प्रश्न उठता है कि लोक अनेक हैं तो क्या सभी लोक स्वतंत्र इकाई हैं। लेकिन ऐसा असंभव है। प्रकृति एक अखण्ड सत्ता है। लोक इसी प्रकृति का ही भाग हैं। ऋग्वेद का पुरुष भी ऐसी ही अखण्ड सत्ता है। सबके भीतर है, सबको आच्छादित करता है। स्पष्ट है कि सारे लोक भी परस्पर जुड़े हुए हैं। पृथ्वी को लोक जानें तो यह जल के नीचे पाताल लोक से जुड़ी हुई है।
पाताल की बढ़ी ऊष्मा से ही धरती कांपती है और भूकंप आते हैं। द्युलोक भी पृथ्वी से संबंधित है। सारे लोक परस्परावलंबन में हैं। मनुष्य और सभी जड़ व चेतन भी। तब इनके भीतर संगति, समन्वय, प्रीति और अनेकता के अंतरंग में एकता की लय भी होनी चाहिए। इसी अंत: एकता की वीणा के सभी तारों की सुर संगति का नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र नमस्कारों के योग्य है और उसका पुत्र जनतंत्र भी। (आईएएनएस/आईपीएन)
(हृदयनारायण दीक्षित वरिष्ठ स्तंभकार और उप्र विधान परिषद के सदस्य हैं )